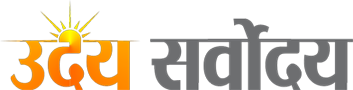शिवानी श्रीवास्तव
यार एक जीवंत, संवेदी और रसमय मूलाधार की वैज्ञानिकता का अक्षुण्ण संचार है। यह मूल रूप से प्रवाही और समुलता में ग्रा‘ होने के साथ ही विज्ञान का भावनात्मक विद्युतीय प्रवाह भी है। इस प्रकार, प्यार स्पष्ट रूप से ‘सिर्फ’ एक भावना नहीं है बल्कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जो कई आयामों में गतिशील और द्वि दिशात्मक दोनों है। यह दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क की संज्ञानात्मकता और शारीरिक प्रक्रियाओं को उद्वेलित तो करता ही है जबकि भावनात्मक और मानसिक अवस्थाओं को भी गहरे प्रभावित करता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्यार दिल से कम और दिमाग से ज्यादा होता है जहाँ हार्मोनल रिलीज और मस्तिष्क रसायन सक्रिय होते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि प्यार होने के पीछे कई हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार होते हैं। जीवविज्ञान में एक दृष्टिकोण यह है कि प्रेम में तीन प्रमुख प्रेरणाएँ होती हैं- आसक्ति, आकर्षण और लगाव। प्राथमिक न्यूरोकेमिकल्स (न्यूरोट्रांसमीटर, सेक्स हार्मोन और न्यूरोपेप्टाइड्स) जो इन प्रेरणाओं को नियंत्रित करते हैं, वे हैं- टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामाइन, आॅक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। डोपामाइन, सेरोटोनिन और आॅक्सीटोसिन कुछ प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि महसूस करने में मदद करते हैं। इसलिए, आपका शरीर अक्सर प्यार को एक चक्र के रूप में देखता है और आप प्यार में बंध जाते हैं।
दूसरे शब्दों में कहे तो जब आपका दिल किसी के लिए धड़कने लगे तो इसका मतलब होता है कि आपको उस शख़्स से प्यार हो गया है जैसा कि बॉलीवुड गानों में बताया जाता है। जबकि यह सबकुछ हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। साफ शब्दों में कहा जाय तो यह साबित है कि जब एक मनुष्य का मस्तिष्क किसी दुसरे मनुष्य के मस्तिष्क के अवयवों की फ्रीक्वेंसी के सातत्य को समरूपता में ग्रहण करता है तो एक विद्युत संचार होता है जो एक-दुसरे के हारमोंस को आकर्षित करने लगते हैं और प्यार हो जाता है। विज्ञान के अनुसार किसी के प्यार में पड़ने के पीछे कई वजह भी यही होती हैं। जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स मजबूत होने लगते हैं और किसी व्यक्ति के प्रति उसका झुकाव बढ़ जाता है। यह आतंरिक संचार जितना अधिक प्रवाल वेग से होगा वह उतना ही अधिक गहरा और समर्पित होता चला जाता है। यही कारण है कि प्रकृति भी अपनी उपदेयाताओं के सकुशल निर्वहन के निमित्ति यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तत्पर रहती है कि हम अपने हार्मोनल रिस्पांस को इस तरह व्यवस्थित करते हुए चले कि आने वाली पीढियां कहीं विलुप्त ना जाएं। यही प्रकृति हमें एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने की अनुमति भी देती है। यह हमारा एक लिम्बिक सिस्टम बनाता है। शुरूआत में यह यौन आकर्षण होता है जिसे हम उस व्यक्ति की ओर महसूस करते हैं, जिससे हम आकर्षण पाते हैं। एस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन इस भावना के लिए जिÞम्मेदार मुख्य हार्मोन हैं।
मूलत: प्यार का विज्ञान एक सारभौमिक, सारगर्भित और प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया है जो धरती पर जीवित रहने, जीवन को उच्चतर अनुभूति देने, संघर्षो से लड़ने और उत्तरजीविता के पायदानों को जीवंत बनाये रखने की आधार ईकाई है। इस अर्थ में प्यार मनुष्य मात्र के लिए अनुकम्पा नहीं बल्कि समस्त प्राणियों में स्नेहसिक्त संबंधों की जननी है। इस प्रवाह की तीनों सीढियाँ (आसक्ति, आकर्षण, और लगाव) उत्तोरोत्तर आगे बढ़ती जाती है और जीवनमूल्यों की गहराई एवं उसके उत्सर्ग की पराकाष्ठा को स्थापित भी करती जाती है। इस अर्थ में प्यार की सार्थकता को बखूबी समझा जा सकता है। जहाँ तक मेरे तर्कों की बात है वह अभिवक्ति की पहचान मात्र है, जो एक मात्र माध्यम हो सकता है यह समझने का कि कैसे आज जीव के जीवंत आधार को बाजार का हिस्सा बना दिया गया है, कैसे उसके इमोसन्सन की बोली लगाईं जा रही है, कैसे वह आतंरिक न होकर बा‘ आडम्बर का एकमात्र बिकाऊ उत्पाद हो गया है? ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के वैचारिक धरातल को काटना चाहता हूँ, और नहीं किसी की अभिव्यक्ति को बांधना चाहता हूँ। क्योंकि न तो मैं प्यार का पहरुआ हूँ, न ही निमित्तिगत विशेषता- जिससे प्यार पहचाना जाय! न मैं प्यार का व्यापारी हूँ न ही मैं उपहारों में प्यार को सिमताने का हिमायती। क्योंकि मेरी नजर में प्यार अपनी मैत्री को बखूबी पहचानता हैं, क्योंकि वह विशेष ज्ञान की निमित्ति उपजा उपहार है- जो सम्रासी धरातल पर सपाट प्रवाह में बहना चाहता है।
सत्य यह है कि प्यार एक स्वच्छंद एवं निरापद भावना है, जिसमें कोई दुराव व लगाव का सीमांकन नहीं होता है। इस अर्थ में किसी से प्रेम करना एक बात है, प्रेम को बाँध कर रखना दूसरी बात है। प्रेम को बांधना, प्रेम करना नहीं है। प्रेम मित्रता के धरातल पर बेहद फलता-फूलता है। क्योंकि प्रेम कभी एकाकी नहीं होता है कि उसे किसी पहचान की जरुरत हो, वह उपजता ही है द्वय की भूमि पर। उसे किसी खास बंधन, किसी खास आकार-प्रकार-व्यापार की बिल्कुल जरुरत नहीं होती है। प्रेम के लिए तो सिर्फ प्रेम का अवयव चाहिए, तत्व का तत्व से मिलन चाहिए। उसे किसी लियाकत की जरुरत नहीं होती है। वह तो आत्मा का परमात्मा से मिलता द्वार है, शरीर का शरीर से मिलन रूपी प्रकृति का नैसर्गिक उपहार है अथवा मस्तिष्क की नाजुक शिराओं से शिराओं के साथ मिलता अदृश्य संगम है। इस अर्थ में प्रेम संगम है, प्रेम समचेतना का संवाही रथ है। प्रेम की रीति, प्रीति और प्रतीति अनुपम है। कब, किससे, किस क्षण, वह बंध जाय, अज्ञात है? बौद्धिकता की सारी दीवारें टूटकर भी उत्तर नहीं दे सकती है- मानव ज्ञान की सारी सीमायें वहां अनुत्तरित ही रह जाती है? प्रेम अत्यंत ही व्यापक तत्व है और व्यापक होते हुए भी बिल्कुल क्षणजीवी भी है। क्षणजीवी होने का अर्थ यहाँ टूटना नहीं है बल्कि उसके साथ जोड़ने के सारे पोषक तत्व हर क्षण मधुमक्खी के छत्ते की तरह कार्यरत रहते हैं, ताकि वह एकसूत्र में तिरोहित हो सके, समाहित हो सके, एक-दूजे को होम कर सके।
हा, यह बिल्कुल सत्य है कि प्रेम हर क्षण परीक्षा लेता चलता है क्योंकि वह घात-प्रतिघात से उपजा तीसरा तत्व है। वह किसी घरौंदें में पला-बढ़ा लता नहीं है जिसे जब चाहा, जहाँ चाहा, उगा लिया। न ही वह गुलाब के फूलों एवं महंगे उपहारों का कर्जदार है, जिसे लेन-देन मात्र से खरीदा जा सके। न ही प्रेम पहचान मात्र का भूखा है। वह तो पलकों पर बसने वाले दृश्यों की धड़कन है जो आहटों पर विश्राम करता है। यहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत की खास पहचान है कि वह भावनात्मक आहटों में कुलांचे भरता है। आज जब सांस्कृतिक विरासत की पहचान ही धूमिल होती जा रही है तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि अपना प्यार कैसे सुरक्षित रह पायेगा? जब इंशानी धमनियां ही दूषित और कलुषित हो जाय तो मूल्यों का रक्षण-संरक्षण-संवर्धन भारी तो पड़ेगा ही। जबकि हमारा भारत एक बहुआयामी, बहुधर्मी, बहुप्रयोगी और बहुप्रतिती संस्कृतियों का बेजोड़ समन्वय है। ऐसे में प्यार की आयातित संकल्पना निजता को दूषित ही करती है। यही कारण है कि नए आगोश में आज प्यार एक ‘प्यार दिवस’ दिवस बन गया है जबकि इससे आगे भी अब यह ‘व्यापार दिवस’ के रूप में स्थापित होता जा रहा है। बौधिक साम्राज्य के साथ-साथ व्यापारिक साम्राज्य की संकल्पना जोर पकड़ती जा रही है। जिसमें सारी मानवीय धड़कने सिमटकर पन्नो पर आ गई है या उपहारों के आईने में देखि जाने लगी है। जहाँ विचारों की कौंध प्राकृतिक रोशनदानों न आकर कृत्रिम रंगों के मृत चमन में पलने लगा है। अब सब कुछ परिभाषित होने लगा है चंद सिक्कों की ठनक पर। जहाँ प्यार अभिव्यक्ति का मूल स्वरुप हो गया है, जिसमें संवेदना का स्थान नामी कंपनियों का हो गया है।
आश्चर्य यह की सदियों से बदलते सांस्कृतिक और रासायनिक प्रयोग प्रेम की रीति-प्रतीति-नीति को नहीं बदल सके, जो क्रोमोजोंस की गुणता के साथं प्रवाहित और सिंचित हो रहा था और होता भी रहेगा, यह सत्य है। लेकिन दुर्भाग्य यह कि कुछ बहुरूपिये इसकी नीति-प्रतीति को बदलने पर आमादा हैं। आज चरों तरफ जाल बिछाया जा रहा है और हम उसके भोजन बनने को तैयार बैठे है। यह कितनी बड़ी बिडम्बना है कि जिस प्यार की पहचान मानवीय गन्धों से होती थी उसे हम तराशने एवं सुसंकृत करने का ठेका कुछ खास व्यापारिक ठिकानों के हाथों सौंप दिए हैं। शायद वे भूल जाते हैं कि यह प्रयास कुछ हद तक सफल तो हो सकते है, वे सीमायें खींच सकते हैं, उसे लिटा सकते है, सुला सकते हैं, रुला सकते हैं लेकिन जब भी प्यार अपने स्वरुप की माँग करेगा सदा ही वह विजेता बन कर रहेगा, उसे सदा के लिए हराया नहीं जा सकता है। क्योंकि यह सत्य है कि संस्कृत और इतिहास के न जाने कितने अध्याय वर्तमान की सीमाओं में व्यतीत हो गए लेकिन आज भी वह अपने वजूद में ही रोमांचित हो रगो में दौड़ना चाहता है। वह बारम्बार पुकारता है अपने धारित्री को, जो जीवन को सीमाबद्ध प्यार के पहलुओं में उसी तरह बांध देना चाहता है, जैसे मकड़ी अपने जले में सभी कुछ बांध लेती है लेकिन स्वयं सदा ही स्वतंत्र रहती है।
प्यार और मनोविज्ञान
मनोविज्ञान के मुताबिक, प्यार एक जटिल भावना है। यह कई भावनाओं और विचारों का समावेश होता है। प्यार में पड़ने पर शरीर में कई बदलाव होते हैं और दिमाग में हार्मोनल रिलीज होती है। अपने अध्ययन के आधार पर विश्व के मशहूर मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बताते हैं कि प्यार के व्यापार में मनोवैज्ञानिक उत्पाद के तीन घटक होते हैं- अंतरंगता, जुनून, और प्रतिबद्धता। जबकि मनोवैज्ञानिक हजान और शेवर के शोध के मुताबिक, सुरक्षित लगाव प्यार की सबसे आम शैली होती है। वे कहते हैं कि प्यार और लगाव में किसी व्यक्ति के अनुभव उसके विश्वासों को प्रभावित करते हैं। जबकि इन प्रभावों का जीवों पर उसके व्यवहार, खानपान, माता-पिता के जीन्स और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता का बहुत असर होता है। यही कारण है कि प्यार में पड़ने पर शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन, और आॅक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय तो हो जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव सभी पर अलग-अलग होता है। जबकि यह भी पूरी तरह सत्य है कि प्यार में पड़ने पर प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में एक साथ एक लाख से ज्यादा न्यूरोट्रांसमिटर सक्रिय होते हैं और उस व्यक्ति, व्यक्तियों और जीव-जंतुओं को अपनी पकड़ में ले लेते हैं। वहीँ, गहरे प्यार में पड़ने पर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक सेकेंड में दस हजार से ज्यादा नए न्यूरोकनेक्शन बनते हैं। यही कारण है कि प्यार में पड़ने पर आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति गहरी भावनाएं महसूस करने लगते हैं। जिसे आसन भाषा में सभी प्यार या मोहब्बत कहते हैं।
प्यार और संवेदना
प्रेम का संवाहक संवेदना ही होती है। वहाँ, प्रेम की संवेदना, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आनंदपूर्ण भावनात्मक संवेदना पैदा करती है जहाँ सच्चे प्रेम में, दोनों पक्ष एक-दूसरे की भावनाओं, विचारों और स्वाभाविक विशेषताओं का सम्मान करना अपना सर्वाधिकार मान बैठते हैं। जहाँ से सच्चा प्यार, पूर्ण विश्वास और कठोर ईमानदारी की व्युत्पत्ति होती है। यही व्युत्पत्ति वह रसायन बनाता है जो जीवन उमंग को रसों से भर देता है और इसके समतल बुनियाद पर रिश्ते निर्मित होते हैं। दोनों पक्षों के बीच आत्मविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है और वे एक-दूसरे की बातों पर ईमानदारी से निर्भर करते हुए जीवन रस में सराबोर हो जाते हैं।
इस अर्थ में प्रेम की गहरी भावना जब दिल की जमीन पर उतरती है तो संवेदनाएं प्रस्फुटित होती है, व्यक्ति मदहोशी में चला जाता है और खोते-खोते विचारों के विपणन में समा जाता है। यह क्रिया जब तक ज्यामितिक रहती है वह प्यार के अंतस्तल को समाया रहता है वहीं जब यह क्रिया अंकगणितीय हो जाती है तो व्यक्ति प्यार के व्यापार के खेल में शामिल हो जाता है। इसमें कई प्रकार की भावनाएं और विचार शामिल होते जाते हैं और वह उथले सागर की तरह स्थिर हो जाता है। जबकि प्रेम की ज्यामितिक संवेदना, हमें दूसरों की मदद करने, उनकी देखभाल करने, और उनके साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस अर्थ में प्रेम से सुख, शांति, और आनंद के अप्रतिम स्रोत की अनुगूँज उठती रहती है। यहाँ व्यक्ति प्रेम में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, और व्यक्ति दयालु, करुणामय, और समझदार बनता जाता है।
प्यार और व्यापार
आधुनिका अर्थ में प्यार और व्यापार एक समानार्थी होकर रह गए हैं। व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं का लेन-देन होता और उसके बदौलत व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्कताओं की पूर्ति करता है या कुछ अंश में मनोवैज्ञानिक जरूरतों की भी संतुष्टि कर पाटा है। लेकिन सपाट स्वरुप में प्यार और व्यापार दोनों में ही आदान-प्रदान, लेन-देन, और विनिमय का हिस्सा होते जा रहे हैं। यहीं कारण है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में प्यार और व्यापार की जटिलता बढ़ती ही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फूलों, तोहफों और ग्रीटिंग्स की बढ़ती उपयोगिता प्यार के निहितार्थ को ही बदल दिया है। आज बाजार में गुलाब का एक फुल प्यार की निशानी बनकर पांच रुपये से लेकर 250 रुपये तक में बिकने को तैयार है। आज बाजार में 1.5 बिलियन कार्ड एक-दुसरे को भेजें जाते हैं जिसकी कीमत 5 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होती है। एक अनुमान के अनुसार मात्र वेलेंटाइन डे पर ही 12 हजार करोड़ रुपये के फूलों एवं कार्डों का व्यापार हो रहा है। इस प्रकार हम इस पुरे व्यापार के वास्तविक टर्नओवर को समझ सकते हैं! इसके माध्यम से एक प्रेमी दुसरे प्रेमी को भेंट करते हैं। दुसरे शब्दों में प्यार बाँटते हैं। लेकिन इतना कुछ होने पर भी प्यार नदारत है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या वास्तव में यह सब कुछ प्यार बांटता है?
प्यार और वेलेंटाइन
प्राचीन रोम में फरवरी का महिना सबसे शुभ मन जाता है। इस समय व्यक्ति अपने घरों की सफाई के साथ ही सामाजिक कार्यों में योगादन देना महत्वपूर्ण मानते हैं। मानसिक और शारीरिक शुद्धता का प्रतीक इस माह के 15 तारीख को छोटे स्तर पर उर्वरता दिवस के रूप में मनाये जाने की परंपरा सदियों से विद्यमान है। एक दिन पहले यानि 14 फरवरी को वहां की सारी यौवनाएं एक बड़े पात्र में अपने संभावित जोड़ी का नाम लिखकर जमा करती थी तथा उसे किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा खोला जाता था। इस प्रकार बने जोड़ों को उस वर्ष का सर्वाधिक पूर्ण जोड़ी का खिताब पहनाया जाता था जिसकी संख्या हजारों में होती थी। इस प्रचाल को देखते हुए वहां के पोप गेलेसियास ने 14 फरवरी को वेलेंटाइन दिवस घोषित किया था जिसे अक्षरश: आज भी शिरोधार्य कर लिया गया है।
दूसरी मान्यता के अनुसार मध्य काल में फ्रÞांस और इंगलैंड में एक धारण बनी की मध्य फरवरी बसंत का मौसम होने के साथ पक्षियों के समाज के साथ अधिक समय देने का होता है। अत: यह धारणा इस विचार को और अधिक मजबूत किया कि यह महिना ईश्वर की कृपा का अनुगृहित है। इसकी पुष्टि प्राचीन ग्रंथों से भी होती है। अत: 14 फरवरी को रोमांस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तीसरी अवधारणा यह है कि 270 ईसवी में संत वेलेनटाईन का देहांत हुआ था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसी के सम्मान में इस दिवस को वेलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
जहां तक ‘वेलेंटाइन’ शब्द की उत्पत्ति की बात है, यह लैटिन के ‘वेलेटिनस’ शब्द से बना है, जिसका मूल शब्द ‘वैलेश’ है। इसका अर्थ होता है- स्ट्रांग, पावरफुल, माईटी। आज के बदलते परिवेश में वेलेंटाइन शब्द का अर्थ भी बदल, भाव भी बदला तथा लोगों की सोंच भी बदली। इस शब्द के व्यापक अर्थ को बाजार ने नयें कलेवर और रूप में सामने रखा जिसे तथाकथित कम्पनियाँ अपना मुखड़ा बना बैठी। आज इसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही है और यह अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमिका जगजाहिर है।