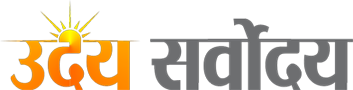अवनीश कुमार गुप्ता
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र में महिलाओं की सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी एक ऐसा विषय है। जो न केवल सामाजिक संरचना की गहराई को उजागर करता है, बल्कि आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक परिवर्तन की संभावनाओं को भी तार्किक रूप से विश्लेषित करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां संख्याओं के साथ-साथ सामाजिक मानदंडों, नीतिगत ढांचे और ऐतिहासिक संदर्भों का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। यदि हम भारत-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं, तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भागीदारी केवल कार्यबल में उनकी उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति के मूल में निहित एक जटिल संरचनात्मक पहलू है। इस संदर्भ में, तार्किकता और गहन विश्लेषण के साथ यह समझना जरूरी है कि महिलाएं इन क्षेत्रों में कितनी प्रभावी हैं, उनकी राह में क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवाचार कैसे उत्प्रेरक बन सकता है।
सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का स्वरूप भारत में पश्चिमी देशों से भिन्न है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी नौकरियां, सार्वजनिक उपक्रम और नीतिगत ढांचे शामिल हैं, जो स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र नवाचार, गतिशीलता और लाभ-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है। इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मापने के लिए हमें संख्याओं की ओर देखना होगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2022-23 के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 37 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा एक सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन जब इसे वैश्विक संदर्भ में रखकर देखते हैं, तो यह दक्षिण एशिया में भी औसत से कम है। यह संख्यात्मक वास्तविकता हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या यह वृद्धि वास्तव में समावेशी प्रगति का परिचायक है या केवल सतही बदलाव का परिणाम है। तार्किक रूप से विचार करें तो यह स्पष्ट है कि संख्याएं केवल एक प्रारंभिक बिंदु हैं; इनके पीछे की कहानी कहीं अधिक जटिल और गहरी है।
सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिति और भी जटिल है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, पर यहाँ भी प्रगति की गति धीमी है। ग्रामीण भारत में पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिए, जहाँ 33% सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम था, पर क्या यह वास्तव में सशक्तिकरण की गारंटी देता है? कई मामलों में देखा गया कि ये महिला सरपंच अपने पति या परिवार के पुरुष सदस्यों के इशारे पर काम करती हैं, जिन्हें “सरपंच-पति” की उपाधि से नवाजा जाता है। आरक्षण एक शुरुआत है, पर सच्चा बदलाव तब आएगा जब समाज महिलाओं को सिर्फ कठपुतली नहीं, बल्कि स्वतंत्र निर्णयकर्ता के रूप में देखेगा। क्या यह मज़ेदार नहीं कि जिस देश में “नारी शक्ति” की बातें गूँजती हैं, वहाँ शक्ति का असली स्वरूप अभी भी पुरुषों के हाथों में कैद है?
अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से इस मुद्दे को परखते हैं। महिलाओं की भागीदारी न केवल सामाजिक न्याय का सवाल है, बल्कि आर्थिक विकास का भी आधार है। विश्व बैंक का अनुमान है कि यदि भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए, तो जीडीपी में 27% की वृद्धि हो सकती है। यह आंकड़ा कोई छोटा-मोटा सपना नहीं, बल्कि एक ठोस संभावना है जो भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बना सकता है। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या हम इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? शिक्षा में लैंगिक असमानता, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे मुद्दे अभी भी बाधा बने हुए हैं। यहाँ नवाचार की जरूरत है—ऐसी नीतियाँ जो न केवल महिलाओं को काम पर लाएँ, बल्कि उन्हें वहाँ टिकने और तरक्की करने का मौका भी दें। मसलन, कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल की सुविधा या लचीले काम के घंटे जैसे कदम छोटे लगते हैं, पर उनके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं।
ग्रामीण और शहरी भारत के बीच का अंतर भी इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ तकनीक और स्टार्टअप्स में अपनी पहचान बना रही हैं, वहीं ग्रामीण भारत में उनकी भूमिका अभी भी खेती, पशुपालन और घरेलू कामों तक सीमित है। शहरी भारत “वर्किंग वुमन” की तारीफ में कसीदे पढ़ता है, पर ग्रामीण महिला की मेहनत को “रोजमर्रा का काम” कहकर नजरअंदाज कर देता है। दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ चाहिए। शहरी क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास पर जोर देना होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) और कौशल विकास की योजनाएँ कारगर हो सकती हैं। यहाँ क्रम का महत्व है—पहले शिक्षा, फिर कौशल, और अंत में अवसर। बिना इस क्रम के, हम सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को समझने के लिए हमें नीतियों और सामाजिक संरचना के बीच के संबंध को विश्लेषित करना होगा। भारत में सरकारी नौकरियां लंबे समय से पुरुष-प्रधान रही हैं, लेकिन हाल के दशकों में मातृत्व अवकाश, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पॉश) और आरक्षण जैसे प्रावधानों ने महिलाओं के लिए इस क्षेत्र को आकर्षक बनाया है। फिर भी, यह प्रश्न उठता है कि क्या ये नीतियां वास्तव में महिलाओं को सशक्त बना रही हैं या केवल उनकी उपस्थिति को बढ़ावा दे रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में शीर्ष पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी न्यून है। इसका कारण केवल नीतियों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक मानदंडों का वह जाल है जो महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं से दूर रखता है। यह एक ऐसी तार्किक विसंगति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता—जब नीतियां समानता की बात करती हैं, तो सामाजिक संरचना असमानता को पोषित करती है। इस विरोधाभास को हल करने के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता है, जैसे कि लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रम, जो केवल कागजी नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से प्रभावी हों।
निजी क्षेत्र में स्थिति और भी जटिल है। यह क्षेत्र भारत में आर्थिक विकास का इंजन है, लेकिन महिलाओं के लिए यह एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर, यह क्षेत्र तकनीकी नवाचार और वैश्विक अवसरों का द्वार खोलता है; दूसरी ओर, यह असुरक्षा, असमान वेतन और कार्य-जीवन संतुलन की चुनौतियां लाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निजी क्षेत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन का स्कोर 100 में से मात्र 25 है। यह आंकड़ा हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या निजी क्षेत्र वास्तव में महिलाओं के लिए समावेशी है या केवल उनकी श्रम शक्ति का शोषण कर रहा है। निजी क्षेत्र में लाभ-केंद्रित दृष्टिकोण अक्सर लैंगिक समानता को पीछे छोड़ देता है। फिर भी, यह क्षेत्र नवाचार का केंद्र भी है। यदि कंपनियां लचीले कार्य समय, बाल देखभाल सुविधाओं और सुरक्षित परिवहन जैसे उपायों को अपनाएं, तो महिलाओं की भागीदारी में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। यह एक ऐसा रचनात्मक समाधान है जो न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र की उत्पादकता को भी बढ़ाएगा।
इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक सामाजिक मानदंडों का दबाव है। भारत में पितृसत्तात्मक संरचना ने लंबे समय से महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा है। यह मानसिकता न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी मध्यम वर्ग में भी गहरी जड़ें जमाए हुए है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अक्षम है। यदि महिलाएं कार्यबल में पूरी तरह शामिल हों, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है, जैसा कि कुछ अध्ययनों ने अनुमान लगाया है। फिर भी, यह संभावना तब तक अधूरी रहेगी जब तक सामाजिक मानदंडों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और सांस्कृतिक पुनर्जनन की त्रयी को अपनाना होगा। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है, लेकिन भारत जैसे देश में, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम है, यह सबसे प्रभावी मार्ग हो सकता है।
राज्य-वार विश्लेषण इस तस्वीर को और स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, केरल जैसे राज्य में महिलाओं की साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी श्रम शक्ति भागीदारी भी बेहतर है। वहीं, हरियाणा जैसे राज्य में लैंगिक असमानता और सामाजिक दबाव के कारण यह दर कम है। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि नीतियों का प्रभाव स्थानीय संदर्भों पर निर्भर करता है। एक समान राष्ट्रीय नीति सभी राज्यों के लिए प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए, हमें एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा, जहां प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए। यह एक नवोन्मेषी विचार है जो भारत की संघीय संरचना के अनुरूप है और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में निर्णायक सिद्ध हो सकता है।
अंत में, हमें यह स्वीकार करना होगा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी केवल एक लैंगिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तार्किकता, नवाचार और भारत-केंद्रित दृष्टिकोण का संगम आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र में नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्र में रचनात्मक समाधान और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन—ये तीनों मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां महिलाएं न केवल भागीदार हों, बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बनें। यह एक ऐसी दृष्टि है जो भारत को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि सामाजिक रूप से भी समतामूलक बनाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संख्याओं से परे जाकर, संरचनाओं को बदलने और सोच को नया रूप देने की आवश्यकता है। यह एक चुनौती है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जहां संभावनाएं अनंत हैं, यह एक अवसर भी है।