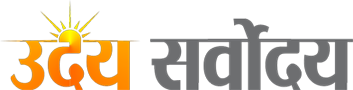हरि भटनागर
सपनों की दुिनया में ब्लैक होल’ संतोष चौबे का हाल ही में आया उपन्यास है. मात्र 132 पृष्ठों का यह उपन्यास उनके खुद के पूर्व में लिखे गए उपन्यासों, कहानियों के मिजाज से थोड़ा हटकर, सूचना तकनीक के मार्फत समकालीन समय के कड़वे सच को उजागर करता है। संतोष चौबे की भाषा में कहें, तो नौ-दस बिन्दुओं के आगे का ऐसा खेल है जिसमें समाज को अस्तित्व में लाने व चेतना सम्पन्न बनाने वाले ब्रेन को लूट की ऐसी धमनभट्ठी में डाला जाता है, जहां उसे, उन सारे सपनों को जलना है जिनमें समाज की बेहतरी के पन्ने झिलमिला रहे थे.
आज जब छद्म नारीविमर्श उथले दलितविमर्श और यथार्थ के नाम पर यथार्थ को धुंधला करती कलाबाजी या आत्म कुंठा और सिर्फ यौनिकता को परोसने का खेल चल रहा हो, तो वहीं पर यह उपन्यास बहुत ही खामोशी के साथ शीर्ष पर बैठे सत्ता के नियंताओं की काली करतूत को जबान देता हिन्दी भाषा की यथार्थवादी परम्परा को रौशन करता यह संकेत कर रहा है कि जब घर में आग लगी हो तो लेखक का दायित्व क्या होना चाहिए?
विषय-वस्तु को समझने के लिए उपन्यास से गुजरें, इसके पूर्व उपन्यास की प्रस्तुति को लेकर पता नहीं क्यों लू शुन की विख्यात कहानी ‘एक पागल की डायरी’ की याद ताजा हो आई है. इस कहानी का पात्र जिन यातनापूर्ण और विषम स्थितियों में सांस ले रहा था, उनको उसने डायरी के पन्नों में दर्ज कर दिया था जिनको उसके साथी ने थोड़ा तरतीब दे दिया था. वे स्थितियां इतनी त्रासद थीं जिनके चलते वह असामान्य होता गया और अंतत: पागल हो गया. कहानी की असामान्य कर देने वाली स्थितियों की अनुगूंज अगर संतोष चौबे के उपन्यास में सुनाई पड़ती है तो यह मान लेना चािहए कि आततायी स्थितियां आदमी को कहीं भी सामान्य नहीं रहने देतीं.
उपन्यास से गुजरते हुए केंद्रीय भाव के रूप में जो बात समझ में आती है, वह है कार्तिक का स्वप्न देखना. कार्तिक का स्वप्न क्या है? उसकी संवेदना क्या है? क्या वह स्वप्न व्यक्तिकेन्द्रित है या समाज के लोगों की बेहतरी की आकांक्षा से प्रेरित है? इन सवालों का जवाब यही है कि उसका स्वप्न समाज के उस युवा के लिए है जो कहीं अलग-थलग पड़ा है जहां विकास की न कोई उम्मीद है और न ही कोई भरोसा. कार्तिक कम्प्यूटर तकनीक के माध्यम से, जो आज के समय की सबसे अहम जरूरत है, उस युवा को समाज की मुख्यधारा में लाना चाहता है. लेकिन वह जानता है कि केवल सूचना तकनीक युवाओं को अस्तित्व में लाने हेतु पर्याप्त नहीं है, आज युवा को मल्टीपरपज बनाना बहुत जरूरी है. इस सोच से भरकर ही कार्तिक एक स्वप्न देखता है :
स्वप्न में वह सपीर्ली सड़कों से होकर गुजरता एक पहाड़ पर चढ़ता जाता है. ऊपर सूरज की स्वर्णिम किरणों से धुली- धुली उसकी चोटी पर पहुंचने के बाद वह नीचे देखता है. भारत के सैकड़ों गांव उसे नीचे बिखरे नजर आते हैं जिनमें कम्प्यूटरों पर बैठे हैं हजारों नवयुवक और नवयुवतियां. वह ऊपर से उन्हें हाथ हिलाता पर वे उसे कहां देख पाते थे? अचानक धीरे-धीरे उड़ते हुए वह उनमें से किसी एक के पास पहुंचा, उसकी पीठ थपथपाता. वह युवक अचानक उसे सिर उठाकर देखता और कहता- सर, आप? इस स्वप्न के बाद एक और दृश्यांतर में जब वह नीचे आता तो लड़के-लड़िकयों का एक झुंड उसे घेर लेता. कई कहते कि उसी के कारण उनका जीवन सुधर पाया है. वह उन्हें किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम के बारे में समझाने लगता. फिर अचानक सब लोग गायब हो जाते, वह अकेला रह जाता वहां कम्प्यूटर पर काम करता हुआ. तब कोई लड़की धीरे से आकर पीछे से झप्पी लेती, झप्प… यू आर ग्रेटर, क्या वह नंदिता थी? कभी पहाड़ से उतरते ही वह अपने आपको समुद्र के किनारे पाता जहां कई लोग उसे पहचान लेते. कुछ सिर्फ मुस्कराते, कुछ कहते- देखो, वह रहा कार्तिक! वह मुस्कराहट का जवाब मुस्कराहट में देता- हाय, ओ हलो, जी, नमस्ते…
पवर्तोें- सी ऊंचाई और समुद्र के विस्तार से अलग, सपनों की एक और श्रृंखला थी जो लकदक होटलों, उच्च स्तर के महाविद्यालयों तथा अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संगठनों तक जाती थी, जहां राजशेखर अपने काम के बारे में बताता, फिर प्रेजेंटेशन करता. आॅडिटोरियम में बैठे लोग उसकी दृष्टि से आश्चर्यचकित होते. कई बार उसे पुरस्कार आदि दिए जाते. अखबारों और मीडिया में उसके साक्षात्कार आते. एक बार तो उसने खुद को यूनाइटेड नेशंस में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर भाषण देते हुए पाया. वह वाकई बड़ा आदमी बन गया था. लेकिन स्वप्न और दु:स्वप्न में भारी अंतर होता है. कहां वह अपने कम्प्यूटर तकनीक के मॉडल को पूरे देश में फैलाकर मल्टीपरपज से लैस युवा को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न देख रहा था, वहीं दु:स्वप्न अनिष्ट की छाया लिए स्वार्थ और कुटिलता से भरा उसके सुखद स्वप्नों के दरवाजे खटखटाता है। मानो कह रहा हो कि अब हमारे रहते तुम्हारी कोई जरूरत नहीं. कार्तिक अपनी सकारात्मक सोच के अपने सपनों को उजड़ने नहीं देना चाहता किंतु दु:स्वप्न का रूप भयावह है :
दु:स्वप्न वास्तव में एक विशालकाय मशीन है जो धमनभट्ठी की तरह है जिसमें एक ओर बहुत से मनुष्य डाले जा रहे हैं, छोटे शहरों के, गांवों के, उसके केन्द्रों की तरह युवा, और दूसरी ओर से पूंजी निकल रही है- सतत प्रवाह के रूप में जो पता नहीं किस अदृश्य हाथों में जाकर गुम हो जाती है! उसके देखते ही देखते वह मशीन एक आटोमेटन में बदल जाती है जिसमें पूरे देश के देश डाले जा रहे थे, उनकी पूंजी, उनका कच्चा माल, उनका आदमी और वे सब उस आटोमेटन में,खींचे जाकर गुम होते जा रहे थे. इधर से हँसते खेलते मनुष्य, हँसते खेलते देश उस मशीन में डाले जाते और इधर से बंजर भूमि, सूखे रसहीन मनुष्य और पूंजी का ढेर निकलता. एक ब्लैक होल जैसा कुछ था जो उन्हें सोख रहा था.. दु:स्वप्न का खेल चलता जाता है. कार्तिक सोचता है कि वह ब्लैक होल की तरफ गया ही क्यों? अपने हजार सेंटरों के साथ वह खुश था, ब्रेनस्टॉरमिंग सेशन, घूमना-फिरना, दिमाग को खाली करने और अनुभवों को बांटने की प्रक्रिया क्या खूब थी! लेकिन आईटी सेल के राजशेखर और विश्व बैंक के झांसे ने उसे कहीं का न छोड़ा! पूरे भारत में अपने मॉडल की पहुंच उसे पेंडुलम की तरह लगी जो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाती. कार्यालयीन यांत्रिकता और न्यायालय की झूठी निष्कर्षहीन लड़ाई …
इस खेल में कार्तिक अंतत: हारता है, झुकता है किन्तु टूटता नहीं. आखिर में कार्तिक प्रतिकार स्वरूप इस दु:स्वप्न से दूरी बना लेता है. यह दूरी ही कार्तिक के सकारात्मक सोच का एक रास्ता है जो उसे पुन: अपने सोच को, स्वप्न को बचाने एवं नई दिशा में विकसित करने में मदद करेगा. यह दूरी ही कार्तिक कथा का नया अध्याय है, बिल्कुल नए जीवन जैसा जिस पर उसे और उसकी टीम को बढ़ना है. स्वप्न और दु:स्वप्न के मार्फत संतोष चौबे ने आज के समय-सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है. स्वप्न एक रचनात्मक सोच है जिसके जरिए आदमी दूसरी किन्तु बेहतर दुिनया को सँजोना चाहता है जिसमें श्रम के मूल्य का आदर हो, सबकी बेहतरी के अवसर हों. वहीं दु:स्वप्न स्वप्न के सोच को खारिज करते हुए लूट-खसोट और उत्पीड़न में भरोसा रखता है। मुक्तिबोध के शब्दों में यह जो पूंजी से जुड़ा मन है यही ब्लैक होल है जिसकी स्याह छाया में आदमी आदमी नहीं रह पाता. संतोष चौबे इस दु:स्वप्न से दूरी का संकेत करते हैं ताकि नई और बेहतर दुनिया का निमार्ण हो सके. जयशंकर प्रसाद याद आते हैं जो कहते हैं :
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे! यह भुलावा दु:स्वप्न से दूरी का संकेत है. यह दूरी कदाचित महात्मा गांधी की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति की वह राह थी जो तोल्स्तोय ने उनके कहने पर उन्हें सुझाई थी. सन 1908 में महात्मा गांधी के अनुरोध के जवाब में तोल्स्तोय ने लिखा था: बुराई का प्रतिकार न करें किन्तु स्वयं बुराई में, प्रशासन, न्यायालयों, कर-संचय और मुख्यत: सेनाओं में हिस्सा न लें, तब दुनिया में कोई भी आपको अपने अधीन नहीं कर पाएगा. ‘सपनों की दुनिया में ब्लैक होल’ अमानवीय व्यवस्था की अधीनता से मुक्ति का संकेत है. यही कार्तिक कथा है. उपन्यास के कुछ नैरो होल्स भी हैं जिनका उल्लेख करना चाहता हूं. ध्यान रहे, उपन्यास का मुख्य पात्र यह वही कार्तिक है जिसने उन नौ बिन्दुओं के खेल से परिचय कराया था, जिसने उद्योगपतियों को धनी और बैंकों को कंगाल बना दिया था जिनमें जनता का पैसा एक सकिंग मशीन की तरह खींचा तो जा रहा था, पर वहां से उसके लौटने की कोई गारंटी नहीं थी…
जब अजय कालिया और नीरज सोनी जैसे लोग बैंकों के हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भागे तो इसी कार्तिक ने लूट के कारनामों का पदार्फाश किया था. तात्पर्य यह है कि कार्तिक कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता था, उसका मुखर विरोध करता था, लेकिन जब भारत सरकार के आईटी सेल और विश्व बैंक की मिलीभगत से उसके अपने मॉडल को हाइजैक किया जाता है और उसे अपना बताकर प्रस्तुत किया जाता है। उस वक़्त विद्रोही कार्तिक चुप रहकर अन्याय सहता क्यों आता है? क्या उसका विरोध सिर्फ सपनों तक ही सीमित रहता है? सपने में ही वह प्रेस कांफ्रेंस के बीच हंगामा खड़ा करता है. त्यागी का गला पकड़ लेता है, राजशेखर के सामने टेबल पर बैठ जाता है-एंकर से पूछता है कि आप चिल्ला-चिल्ला कर इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? उस वक़्त उसे देशद्रोही तक कहा जाता है. और इस देशद्रोही जिसकी दुर्गम से दुर्गम डाकू और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बीच गहरी पैठ है जहां उसके अपने कम्प्यूटर सेंटर्स के साथी- संघाती हैं जहां से विरोध की बहुत बड़ी आवाज उठ खड़ी हो सकती है, भले ही उसे दबा दिया जाए! दूसरे कार्तिक ऐसा चमत्कारी उद्यमी लगता है जो विषम से विषम स्थितियों में भी पेंचों से भरे प्रोजेक्टों को किसी जादू की तरह अंजाम दे देता है. और विजयश्री उसके हाथ आती जाती है. यहां वे सूत्र गायब हैं जो विजयश्री के पहले अड़चन के रूप में आड़े आते हैं. इन पर विचार करना जरूरी है.
बहरहाल, इन नैरो होल्स के बावजूद संतोष चौबे का उपन्यास इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें समकालीन समय के जलते सवालों को ढांका-मूंदा नहीं गया है, उनको बेबाकी से उजागर किया गया है. भले ही उसमें कुछ झोल हों, किन्तु मंशा पूरी तरह पाक- साफ और ईमानदार है.