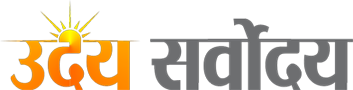विजय गर्ग
अभिव्यक्ति के हर माध्यम की अपनी चरित्रगत विशेषता होती है। साहित्य में लेखक अदृश्य बिंबों का सृजन करता है, जबकि सिनेमा पूर्णत: दृश्य माध्यम है। इसलिए साहित्य का सिनेमा में रूपांतरण सीधे-सीधे अदृश्य का दृश्यों में रूपांतरण होता है। वह भी कला या मूर्तिकला की तरह एक स्थिर चाक्षुष बिंब भर में नहीं, बल्कि पूर्णत: जीवंत और प्रत्यक्ष नजर आते जीवन के घटनाक्रम में। जाहिर है कि यह रूपांतरण अतिरिक्त संवेदनशीलता और अपने माध्यम में गहन निपुणता की मांग करता है, और इस हद तक सृजनशीलता की, कि जैसे फिल्म का निर्देशक उसे अपनी ही मौलिक कृति की तरह रचे।
एक व्यक्ति जब पाठक के रूप मे साहित्य पढ़ता है, तो वह अनायास स्वयं उस सृजन प्रक्रिया से संबद्ध हो जाता है। लेखक शब्दों के माध्यम से उसके सामने जो चरित्र प्रस्तुत करता है, उसे वह अपनी तरह से, अपनी कल्पना में सृजित करता है। उसके सामने जो घटनाएं लेखक प्रस्तुत करता है, उन्हें वह स्वयं अपनी कल्पना में आकार देता, और उन्हें घटते हुए देखता है। इस तरह सृजन की एक प्रक्रिया, जो लेखक द्वारा शुरू की जाती है, वह व्यक्तिगत रूप में ही सही, पाठक की कल्पना में साकार होकर पूर्ण होती है। वही व्यक्ति जब फिल्म देखता है, तो उसकी सृजन प्रक्रिया से संबद्ध नहीं हो पाता। इसलिए कि उसके चरित्र अपने पूरे रूप और साज-सज्जा में उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। संपूर्ण घटनाक्रम बना कर उसकी आंखों के सामने चलती-फिरती-बोलती वास्तविक जिंदगी की तरह दिखाया जाता है। बेशक वह फिल्म निर्देशक की कल्पना पर आधारित होता है। लेकिन उन्हें सृजित करने में दर्शक की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। उसे महज देखना और देख कर पसंद या नापसंद करना होता है। पुस्तक पढ़ कर उसने अपनी कल्पना में जो बिंब सृजित किए होंगे, अगर सिनेमा के बिंब उनके अनुरूप या बेहतर हुए, तब तो वह उसे पसंद कर पाता है अन्यथा नहीं। लेकिन इससे इतर एक बड़ा दर्शक वर्ग वह होता है, जिसने साहित्य में उसे नहीं पढ़ा होता है। वह सीधे उस कहानी का परदे पर ही साक्षात्कार करता है। उसकी स्वीकृति सीधे इस पर निर्भर करती है कि निर्देशक उस साहित्य के कथानक, संवेदना और भावों को कितनी सफलतापूर्वक फिल्म में उतार पाया है। अगर बाहरी दबावों के चलते उसने अनावश्यक समझौते कर लिए हों, तो जाहिर है कि फिल्म अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाती।
साहित्य में सहूलियत यह है कि लेखक पृष्ठ-दर-पृष्ठ चरित्रों के मनोभावों में गहरे उतरता चला जा सकता है, जैसे निर्मल वर्मा के गद्य में होता है। जबकि सिनेमा को अपने पात्रों के मनोभावों को प्रकट करने के लिए उसके चेहरे पर नजर आते भाव ही पकड़ने होते हैं। वह सिर्फ बाहरी बिंब पकड़ सकता है। उसके मन के भीतर नहीं उतर सकता। लेकिन उसके पास चलते-फिरते चाक्षुष बिंब हैं, आवाज है, लाईटों के प्रभाव हैं, और अब तो आधुनिकतम तकनीक भी है, जो दृश्यों को शब्दों की बनिस्बत अधिक सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।
सामान्यतया जिस दृश्य या भाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक को विस्तार में जाना पड़ता है, उसे कैमरा महज एक क्षण में अधिक वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। साहित्य के पाठक के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। वह एक ही पुस्तक को कई दिनों तक पढ़ता चला जा सकता है, बल्कि अनेक बार पढ़ सकता है। एक तरह से वह कृति उसकी संवेदना का हिस्सा हो जाती है। जबकि सिनेमा के सामने उसी कृति को महज ढाई घंटे में प्रस्तुत करने की सीमा होती है। ऐसा करने के लिए उसे बहुत से विस्तार और अंशों को भी उसमें से निकाल देना होता है। साथ ही चुनौती यह भी होती है कि ये तमाम परिवर्तन करते हुए साहित्यिक कृति की मूल कथावस्तु, मूल भावना और मूल संवेदना के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। अगर यह जरूरी संवेदनशीलता के साथ नहीं किया गया, तो फिल्म न तो अपेक्षित प्रभाव छोड़ पाती है, न साहित्यिक कृति के साथ न्याय कर पाती है। बावजूद ऐसी अनेक कठिनाइयों और सीमाओं के, साहित्य का फिल्मों मे रूपांतरण होता है। अंग्रेजी में बड़े पैमाने पर होता है। वहां तो जैसे परंपरा-सी है कि क्लासिक कृतियों पर आधारित क्लासिक फिल्मों का निर्माण हो जाता है, और वह भी वैसी ही भव्यता, समझ और गुणवत्ता के साथ, जैसी रूपांतरण से अपेक्षित होती है। वे स्वयं प्रस्तुतीकरण और कला की उन ऊंचाइयों को छूती हैं, जैसी स्वयं साहित्यिक कृति। आॅस्कर अवार्ड प्राप्त फिल्मों में बड़ी संख्या साहित्यिक कृतियों से रूपांतरित फिल्मों की है।
फिर हिंदी में कहां बाधा आती है? होता है रूपांतरण, लेकिन बहुत कम होता है उसका अनुपात। शरतचंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या अमृता प्रीतम आदि पर अवश्य कुछ अच्छी फिल्में बनी हैं। लेकिन फिल्मों को बेहतरीन कथानकों की जरूरत होती है, और हिंदी साहित्य में ऐसे कथानकों का भंडार उपलब्ध होता है, जो फिल्मों से अछूता रह जाता है। समांतर फिल्मों के दौर में अवश्य आशा बंधी थी कि सामाजिक समस्याओं से जूझती गंभीर कलात्मक फिल्मों के युग का आगाज होगा, और वे तत्संबंधी साहित्यिक कृतियों को आधार बनाएंगी। कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में आर्इं भी। लेकिन वह दौर दूर तक नहीं जा सका। हिंदी में फिल्मों को महज एक मनोरंजन का साधन मान लेने की जो अवधारणा बनी हुई है, वह गंभीर साहित्यिक कृतियों के फिल्मांकन में बाधा बनती है। फिल्मों को एक व्यवसाय मान कर, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा कर, उसी अनुपात में मुनाफा कमाने की जो व्यावसायिक बाध्यताएं हैं, और उनके चलते जो तमाम तरह के अनुचित समझौते होते हैं, वे उन्हें साहित्यिक कृतियों के फिल्मांकन के लिए प्रेरित ही नहीं कर पाते। ऐसा करते समय वे दर्शकों की रुचि को भी खासा कमतर आंकते हैं। जबकि ऐसा है नहीं। जब भी किसी बेहतरीन कहानी पर लीक से हट कर बनी फिल्म आती है, तो दर्शक उसका स्वागत ही करते हैं। इससे आशा बंधती है कि आने वाले समय में साहित्यिक कृतियों के अधिक फिल्मांकन के लिए उर्वरक जमीन तैयार हो रही है।
हालांकि धार्मिक साहित्य पर अवश्य सफल फिल्में बनती रही हैं। बल्कि रामायण और महाभारत पर बने धारावाहिकों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। लेकिन साहित्य तो अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, और अपने समय का प्रतिबिंब होता है। वह समकालीन समाज में मूल्यों के ध्वंस, मानवीय संबंधों के क्षरण और संस्कृति के अवमूल्यन को प्रतिध्वनित करता है। वह एक भयावह समय को बेनकाब करता है। फिर सिनेमा भी तो अपने समय का प्रतिबिंब होता है। ‘मनोरंजन का साधन’ वाले उसके भाग को छोड़ भी दें, (जो आवश्यक भी है और जिसके स्तर पर ध्यान देना वांछनीय) तब भी उसके दूसरे गंभीर पहलू से गहन सामाजिक यथार्थ का संप्रेषण अपक्षित है। ताकि साहित्य की ऐसी तमाम चिंताओं का उस सशक्त माध्यम में अधिकाधिक समावेश हो और वह अपने अपार दर्शकों के बीच उन अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। आवश्यकता है साहित्य के साथ उसके और अधिक घनिष्ट संबंधों की। इस बात पर गहन मंथन अपेक्षित है कि जो प्रतिबद्ध और समर्पित फिल्मकार जोखिम उठा कर साहित्य से रूपांतरित ऐसी फिल्मों का निर्माण करने का साहस करते हैं, उन्हें कैसे अधिक से अधिक आर्थिक और अन्य किस्म का संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे फिल्में वृहत्तर दर्शक वर्ग से जुड़ सकें।